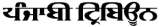लोक,लीक बिन कैसी लक्ष्मी
कुछ दशक पहले की दिवाली की बात करें तो झोंपड़ियों से लेेकर अट्टालिकाओं तक कुम्हारों के बनाए दीये मुस्कुराते थे। हमारी माटी से जुड़े ये दीये ज्ञान, ध्यान, जीवन ज्योति, सिद्धि का प्रतीक कहलाते थे। अब चाइनीज लाइटों की चकाचौंध से चुंधियाई रहती है दिवाली। पहले इस पर्व में लोक-लक्ष्मी का पूजन होता था।
कुछ दशक पहले की दिवाली की बात करें तो झोंपड़ियों से लेेकर अट्टालिकाओं तक कुम्हारों के बनाए दीये मुस्कुराते थे। हमारी माटी से जुड़े ये दीये ज्ञान, ध्यान, जीवन ज्योति, सिद्धि का प्रतीक कहलाते थे। अब चाइनीज लाइटों की चकाचौंध से चुंधियाई रहती है दिवाली। पहले इस पर्व में लोक-लक्ष्मी का पूजन होता था। लोक-लक्ष्मी मायने अन्न, दूध-पूत, पशु-शक्ति, शरम-लिहाज, लोक-मर्यादा, भलमनसाहत, छैल-छबीले गबरू, शर्मीली छोरियां। आज के दौर में दिवाली पर धन-संपदा और वैभव को पूजने का चलन है। कितना बदल गया है दिवाली का स्वरूप, आइए जानें इस आलेख में-
राजकिशन नैन
इन दिनों दीपावली भले ही धन-संपदा एवं वैभव के प्रदर्शन का अशिष्ट उत्सव हो पर असल में यह हमारी कृषि-कुसुमित संस्कृति की स्तवनीय सुषमा का शुभ्र श्लील त्योहार है। सालभर की कठिन मेहनत के बाद घर में आई ‘अन्न-धन’ रूपी लक्ष्मी का सत्कार करने के लिए हम घर-आंगन और कोठार को लीप पोतकर स्वच्छ-शोभन करते हैं और कंगाली के कूड़े-कर्कट को झाड़-बुहारकर एक ओर फेंक देते हैं। खेती-बाड़ी की साख बढ़ाने वाले इस देसज त्योहार को मनाने की शुरुआत सदियों पहले खेतिहर लोगों ने की थी। तभी आम लोगों यानी किसानों की सहयोगी जातियों ने दिवाली मनानी आरंभ की। शरद की सोहन ऋतु में, खरीफ की फसल का नया अन्न घर आने की खुशी में किसान इस दिन माता अन्नपूर्णा की आवभगत करते हैं। अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा का अनुग्रह किसानों पर बेणु के पुत्र पृथु (त्रिशंकु के पिता) के समय से चला आ रहा है। जो लोग दिवाली को वैश्यों का त्योहार मानते हैं, वे भ्रम में हैं। देवी अन्नपूर्णा अर्थात अन्नलक्ष्मी की कृपा वैश्यों यानी व्यापारियों पर कभी नहीं रही। आढ़त और बणज के बहाने किसानों की जिंस पर काबू करने के बाद अन्नलक्ष्मी व्यापारियों के हत्थे चढ़ी है। असलियत में तो वह किसानों की गाढ़ी कमाई की प्रतीक है। लक्ष्मी वास्तव में नाज-पात, फल-फूल, औषध एवं नाना पदार्थों के रूप में खेतों में उपजने वाली शस्य की देवी ‘श्री’ है। किसान पृथ्वी का सच्चा पूत है। किसान की मेहनत और उसकी भलमनसाहत के बूते पर पृथ्वी ठहरी हुई है। किसान के खेत में एक सौ एक प्रकार की लक्ष्मी जन्मती और प्रफुल्लित होती है। गेहूं और चावल के कच्चे दानों में उफनते हुए क्षीर सागर में जनपदीय श्री का सच्चा वास है। गये जमाने में हिन्दी पट्टी के गांवों की खेतिहर स्त्रियां धान की बालियों की श्रीदेवी बनाकर, उसको सिर पर धरकर गीत गाती हुई चाव से धान्य की कटाई किया करतीं। हमारे बड़ों ने लक्ष्मी के जो आठ रूप गिनाए हैं, उन्हें हम अन्न लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धीरज लक्ष्मी, औलाद लक्ष्मी, सूर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और राज लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। इनमें अन्न लक्ष्मी सर्वोपरि है। किसान की निगाह में अन्न सबसे बड़ा धन है। बांगरू की कहावत है— ‘अन्न धन सो अनेक धन, सोन्नों-चांदी आधे धन।’ अर्थात सोने-चांदी को किसान आधा धन मानते हैं। हमारे किसान अन्न को परमात्मा मानते हैं— ‘अन्नं ब्रह्म।’ इस अन्न को किसान उपजाता है। इसलिए किसान महाब्रह्म के रूप में सदा पूज्य है। ग्राम्यांचलों के करोड़ों किसान अन्न देने वाली धरा को साक्षात लक्ष्मी मानते हैं और इसकी कोख से निकसे हुए अन्न को प्रसाद समझकर चुचकारते हैं। हमारे पूर्वज इसी लक्ष्मी यानी भूदेवी को पूजते आए हैं। धरती पर पांव रखने की विवशता के लिए हमारे पुरखे सदैव उससे माफी मांगते थे। वे धन की अपेक्षा धर्म को महत्व देते थे।
पुराकाल में हमारे यहां लक्ष्मी का एक भी मंदिर नहीं था, लक्ष्मीनारायण मंदिर अवश्य थे। भू-देवी कब और कैसे धन की देवी बनी, यह शोध का विषय है। महालक्ष्मी के सब मंदिर उपभोक्ता संस्कृति पनपने के बाद बने हैं। वेदों में भू-देवी की पहचान धन की देवी के रूप में नहीं की गई। इस रूप में सर्वप्रथम उसका जिक्र ‘श्रीसुक्त’ में हुआ है, जो ऋग्वेद का परिशिष्ट बताया जाता है। यह किसने कब लिखा और कैसे इसे वेद में जोड़ा, कोई नहीं जानता। किसानों के देश में भू-देवी को धन का मुकुट पहनाकर धूमधाम से उसकी पूजा-अर्चना करना इस बात का द्योतक है कि सत्ताधीशों, धनपतियों और नौकरशाहों ने खेती-किसानी और भारतमाता ग्रामवासिनी की हद से ज्यादा बेहुरमती की है। नयी फसल के स्वागत से जुड़ा होने के नाते लोक में दिवाली नवधान्येष्टि त्योहार के रूप में मशहूर है। नये अन्न के आने की खुशी में इसे मनाये जाने के संकेत गांवों में कदम-कदम पर मिलते हैं। यह सामणू (खरीफ) फसल के घर आने और साड्ढू यानी चैती (रबी) की फसल बोने का समय है। दशहरे और दिवाली से पूर्व अक्सर ‘धनकोर’ यानी पछवा हवा बहती है जो जीव-जगत एवं फसल आदि के लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। गांववासी इसे अतीत नीरोगी बताते हैं। दिवाली तक किसानों के ठेक्के, बखारी ज्वार-बाजरे से भर जाते हैं। मूंग-मोठ और धान भी सहन में आ चुके होते हैं। गन्नों में मिठास भर जाती है। दशहरे वाले दिन गांवों में ‘पंचगंडा’ पाड़ने की रीत है। पकी हुई पीली कचरियों की खसबोई वातावरण का मिज़ाज मननीय बना देती है। किरे हुए कातकू कचरों को देखते ही लार टपकने लगती है। पर्यावरण को संतुलित करने वाले इस महात्योहार का आगमन शरद की सुहानी ऋतु में होता है। गांववासी शरद को उत्सवों की ऋतु कहकर पुकारते हैं। शरद के सारे उत्सव प्रकृति से जुड़े हैं। खेती करने वाले इन पर्वों के जरिये प्रकृति के प्रति आभार जताते हैं। ग्रामजनों की दिवाली में माटी की महक रमी हुई है। माटी की इस पुष्कल महक की खातिर बचपन में हमें सालभर दिवाली का इंतजार रहता था। घरू कुम्हार द्वारा निर्मित माटी के खिलौने हमें इसी रोज मिलते थे। पचासेक साल पहले तक दिवाली मनाने के लिए सर्वप्रथम माटी की जरूरत पड़ती थी। तब, गांवों में सर्वत्र कच्चे घर होते थे। चौमासे में इनकी हालत बड़ी दयनीय हो जाया करती। छतें तो टपकती ही, दीवारों के ‘ले’ भी उतर जाते। घरों का हुलिया बदरंग हो जाता। दिवाली से डेढ़ माह पहले मेरे पिताजी खदानों से पीली माटी का ‘रैहड़ू’ भरकर ले आते। एक बैलगाड़ी काली मिट्टी की लाते। मेरी मां घर की साफ-सफाई और लिपाई-पुताई करती। वह दशहरे से पांच-सात दिन पहले तक घर को चमकदार बना देती। हमारे बड़ों ने दशहरे से दिवाली तक के दिन मकानों की शुद्धि एवं मरम्मत के लिए तय कर रखे हैं ताकि जहरीले कीड़े-मकोड़े और हारी-बीमारी घर से दूर रहे। इस नाते दिवाली हमारी पर्यावरण शुद्धि की परंपरा का प्रतिनिधि पर्व है। यह हर साल स्वच्छता का संदेश देने हमारी देहरी पर आता है। चौमासे के बाद घर की सफाई का वैज्ञानिक महत्व है। दिवाली के घी-तेल के दीयों के धुएं से बारिश में पैदा तमाम कीट-पतंगे मर जाते हैं। इस दृष्टि से दिवाली कीट नियंत्रण का सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली को प्रकाशपुंज के साथ पर्वपुंज के नाते भी जाना जाता है। गांवों में दिवाली का पखवाड़ा चौदह दिन का होता है जो कातिक बदी चौथ से लेकर कातिक सुदी दूज तक रहता है। इस दौरान आठ शृंखलाबद्ध त्योहार एक साथ मनाने का चलन है। इन सब त्योहारों के लिए माटी के करवा, कमोई, काप्पण, कुल्हड़, कुल्हिया, माट, दीये, दीवड़ी, हीड़ो, मूर्ति एवं बच्चों के खेलने के खिलौने हमारे घरू कुम्हार बनाते थे। ‘वैश्विक गांव’ की अवधारणा से पूर्व झोंपड़ियों से लेकर अट्टालिकाओं तक कुम्हारों के बनाये दीये मुस्कुराते थे। उन दिनों कुम्हार दिवाली की कमाई पर सालभर चुपड़ी खाते थे। तब, घर के सब बर्तन माटी के होते थे। मेरा ताऊ देस्सू माटी के बर्तनों की लोच को इस्पात की लोच से ज्यादा मजबूत बनाया करता। माटी की कढ़ावणी में पका दूध, बिलोवणी में जमाई गई दही, हांडी में रंधी हुई खिचड़ी एवं राबड़ी, बरोल्ली में रंधा साग, घीलड़ी में रखा घी और झाकरे में भरा शीरा सुगंध, स्वाद व गुणवत्ता की दृष्टि से बेजोड़ होता था। कद्दू, घीया, बथुए और ग्वार की फलियों के रायते में जब मेरी ताई डीघलो माटी के चीघसे से छौंक लगाती तो सारे मोहल्ले में खुशबू फैल जाया करती। प्लास्टिक, शीशे और एल्यूमीनियम के बर्तनों ने वह लजीज खाना हमसे एक ही झटके में छीन लिया। माटी के बर्तनों एवं दीयों आदि के बदले में कुम्हार थोड़ा-बहुत अनाज ले लिया करते। दिवाली के पर्वों में सर्वप्रथम कातिक बदी चौथ को ‘करुवा चौथ’ का पर्व आता है, जो वर्षा का पानी निथरने के एवज में मनाया जाता है। इस दिन वर्षा का निथरा जल नये करवों में भरकर नाते-रिश्तेदारों के संग उनकी अदला-बदली की जाती है। सगे-संबंधियों के यहां से आए जल और फल आदि को जमीन पर रखकर दीवार पर अहोई माता का चित्र उकेरा जाता है। नये सूत के लच्छे बच्चों के हाथ-पांवों, कमर व गले में पहनाते हैं। अन्न-पानी की इस अदल-बदल से मेल-मिलाप बढ़ता है। कातिक बदी अष्टमी को अहोई का व्रत रखने की रीत है। कुटुंब में विवाह अथवा पुत्र जन्म होने पर दो मुंह की अहोदी चीती जाती है। अहोई संतान देने वाली माता मानी जाती है। स्त्रियां ‘अहोई का व्रत’ तारे देखकर खोलती हैं। कातिक बदी द्वादशी के दिन ‘छाज द्वादशी’ का त्योहार पड़ता है। छाज, सारा साल हमारा अन्न फटकारता है। उसी एहसान के एवज में हम छाज को याद करते हैं। कातिक कृष्णा त्रयोदशी को ग्रामवासी देव वैद्य धन्वंतरि की धोक मारकर घूरे पर आटे का चौमुखा दीया जलाते हैं। लोहे, कांस्य, भरत एवं पीतल के बर्तनों की लेवा-बेची करते हैं। लोक में यह दिन धन-तेरस के नाम से प्रसिद्ध है। कातिक कृष्णा चौदस को गिरड़ी यानी छोटी दिवाली का त्योहार आता है। गिरड़ी के दिन गांवों में घरू जुलाहे के हाथ के बने लट्ठे से मोटे कपड़े पहनने की रीत सदियों तक रही। घर के सबसे छोटे-बड़े इस शकुन को निष्ठा से पुगाया करते। दीये जलाने की शुरुआत भी गिरड़ी की रात को की जाती है। गिरड़ी के मौके पर देश में नाथ सम्प्रदाय के डेरों में शिव के अवताररूप माने जाने वाले भैरों के नाम का रोट लाजिमी तौर पर बनाया जाता है। दिवाली की सुबह इस रोट का प्रसाद लेने के लिए इन डेरों में देहातियों के ठठ रुपते हैं। गिरड़ी पर मोरी के नाम का ‘जमदीया’ ग्रामीण जरूर जलाते हैं।
दिवाली की जगमग कातिक कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या को होती आयी है। दिवाली पर धनधारी लोग बेशक धन की देवी लक्ष्मी के आगे औंधे पड़ते हों, लेकिन ग्रामवासी अलग और खास अंदाज में दिवाली मनाते हैं। देहात में लक्ष्मी पूजन की प्रथा कभी नहीं रही। गांवों में दो पीढ़ी पूर्व तक लक्ष्मी (विष्णु पत्नी) की जगह घर-घर श्यौरती पुजती थी। दीयों की जग-मग के त्योहार दिवाली से दस दिन पहले चंदन कुम्हार की पत्नी हमारे घर छोटे-बड़े दीये, कुल्हिया, माट, हीड़ो और खिलौने दे जाती थी। मेरी मां दीयों के लिए लोगड़ की बाती दिवाली से दो-तीन रोज पहले बांट दिया करती। हम दीयों को पानी में भिगोते। पानी में भीगे दीयों की मटिया महक घर-आंगन में पसर जाती। भीगे हुए दीये कम तेल सोखते। दीयों के लिए कच्ची घाणी वाला सरसों का तेल हम अपने घरू तेली लीलू के कोल्हू में निकलवाया करते। उस तेल की चमक, गंध और ज़र्द रंग देखते ही बना करता। दिवाली पर हम सब भाई-बहन आधी रात तक दीयों के साथ हर्ष-मग्न रहते। जलते दीयों की ‘चंगेर’ की जगमगाहट देख-देखकर हमारी आंखों की ज्योति सवाई हो जाती। चार जमात तक की स्कूली पढ़ाई हमने माटी के इन्हीं दीयों की रोशनी में पूरी की थी। सरसों के तेल के दीयों की चिकनाई को सांप चाव से चाटते हैं। मेरा चाचा टेकूराम बताया करता कि दिवाली के दीयों की चिकनाई चाटकर सांप शयन करने हेतु जमीन के नीचे चले जाते हैं। मेरा ताऊ रणजीत अन्न एवं जल के बाद दीये के प्रकाश का तीसरा स्थान बताया करता। वह दीये को ज्ञान, ध्यान, जीवन ज्योति, औलाद, खुशहाली, सिद्धि एवं आंखों की रोशनी का प्रतीक कहा करता। मेरी नानी सरसों के तेल के दीये की लाै पर लोहे का पलटा औंधा करके आंखों का काजल बनाया करती तथा रोशनी तेज करने के लिए उसे नित्य हमारी आंखों में आंजा करती। दीये-बाती से जुड़ी कथाओं, कहावतों, किस्सों और गीतों के साथ हमारा भावनात्मक लगाव है, क्योंकि दीपक हमारी उर्जस्वल माटी के नाती हैं। पहले दिवाली के दीयों के साथ ‘हीड़ो’ भी जलायी जाती थी। हीड़ो शब्द हीड़ से बना है, जिसका अर्थ प्रकाश है। दिवाली पर हम कागज, बांस, झाड़ू की सींक, धागे व गोंद की मदद से रंग-बिरंगे कंदील बनाया करते। दिवाली पर घर वाले हमें बुगटे भर-भर खील-खिलौने दिया करते। खीलों में धान की महक और खिलौनों में गन्नों की मिठास भरी होती थी। बम-पटाखों का प्रदूषण तब गांवों में नहीं था। हमें केवल फुलझड़ी, अनार एवं चरखे-चरखी जलाने की छूट मिलती थी। घर की दीवार पर बनी श्यौरती हमारे लिए कौतूहल का विषय होती थी।
मेरी दादी की बनायी श्यौरती की याद मुझे नहीं है। पर मेरी मां बसंती और मेरी मासी गंगा द्वारा निर्मित की जाने वाली श्यौरती का मुझे खूब स्मरण है। गोबर लिपी दीवार पर चावल के घोल से दो सीधी-सरल नारी आकृतियां श्यौरती के रूप में अंकित की जाती। उनके चारों ओर गेरू से चौकोर आकार बनता, जिसके ऊपर हलुए से मौली की माला लगायी जाती। श्यौरती की मूर्ति के नीचे जतन से माटी के गणेश, लक्ष्मी, गूजरी, खील-बताशे भरी डालड़ी, नयी नकोर डाभ की मांज्जण जचायी जाती। साथ में सतनाज्जा (धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उर्द, गेहूं) की सात ढेरियां होती। थाली में पूजन सामग्री के साथ चांदी का एक रुपया रहता। दिनभर के कड़े बरत के बाद मेरी मां पूजा का काम निपटाती। श्यौरती पूजने के बाद घर के तमाम सदस्य बड़ों के पैर छूते। बड़े उन्हें आशीष देते। मेरी मां श्यौरती को सौरती कहती। जब मैं श्यौरती की बाबत पूछता कि ‘मां ये कौन हैं?’ तो मेरी मां उन्हें ‘लोक लिछमीं और सुरस्ती’ बताती। भाषा शास्त्री व लोक संस्कृति सचेतक श्यौरती को बेशक ‘शस्त्र रात्रि’, ‘शरद रात्रि’ अथवा ‘स्यावड़ रात्रि’ जैसे किसी नाम से पुकारें, पर ग्राम समाज इसे लोक लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजता आया है। साठ के दशक तक अन्न-धन, दूध-पूत, पशु शक्ति, देशज हुनर, दातारी, शरम-लिहाज, लोक मरजाद, लोक शील, भलमन साहत, छैल-छबीले गभरूओं और हट्टी-कट्टी शरमाऊ बहु-छोहरियों के रूप में जिस लोकलक्ष्मी के दर्शन देहात में पग-पग पर होते थे। वह लक्ष्मी गांवों में अब कहीं दिखाई नहीं पड़ती। कहां गई वह लोकलक्ष्मी? कातिक सुदी प्रतिपदा को ग्रामीण गोवर्धन यानी गोधन का त्योहार मनाते। तब, घर-घर गाय थी। गाय से खेती खातिर बैल मिलते। खाने को दूध, दही, घी मिलता। घास खाकर गाय जो गोबर करती, उससे उत्तम खाद बनता। गोबर के उपले ईंधन का काम देते। आयुर्वेदिक औषध भस्में उपलों में फूंकी जाती। उपलों की राख चेचक के घाव सुखाती। ताजा गोबर पित के ददोड़ों को ठीक करता। उपलों का अंगार गुम चोट को हरता। उपलों की राख से बर्तन मंजते। उपलों की आग से चिलम सुलगती। उपलों की आंच में दूध पकता। उसी में खीर, दलिया, खिचड़ी व साग रंधता। गोबर से चूल्हा-चौंका चांदी-सा चमकता। गोबर के अगणित उपकारों के एवज में उसका मान रखते हेतु गोवर्धन के दिन गोबर की आदमकद मूर्ति बनाकर पूजी जाती। तब, देश में गोधन का बाहुल्य था। कातिक सुदी दूज को ‘भाई दूज’ पर्व मनाते।
आज गांवों में न वह लोकलीक है, न वैसी दिवाली है। कुलक्ष्मी ने लोकलक्ष्मी एवं सरस्वती के घर ढहा दिए हैं। हरित क्रांति ने पशुधन एवं पशुओं की खेती उजाड़ दी। धन लक्ष्मी की चकाचौंध ने पुरखों का तमाम पुरुषार्थ माटी में मिला दिया। ऋतु, पर्व, मंदिर, देवी-देवता, अवतार और महापुरुषों की ओर अब कोई नहीं देखता। दिवाली का मंगल उजियाला आधुनिकता की आंधी में धूमिल पड़ गया है।